

| स्वयंभू ब्रह्मा | स्वायंभुव मनु | ब्रह्मर्षि अंगिरा |
| महर्षि अंगिरा | महर्षि अथर्वागिरस (अथर्वा) | देवगुरु बृहस्पति |
| सृष्टि रचयिता विराट विश्वकर्मा | आदि शिल्पाचार्य भौवन (भुवन) विश्वकर्मा | विश्वकर्मा का देवकार्य में सहयोग |
| वसुपुत्र विश्वकर्मा | भृगुवंशी विश्वकर्मा | सुधन्वा विश्वकर्मा |
| विश्वकर्मा जी की अवधारणा | विश्वकर्मा अवतार | वंशावली |
| वेदों में विश्वकर्मा | विश्वकर्मा संतति |
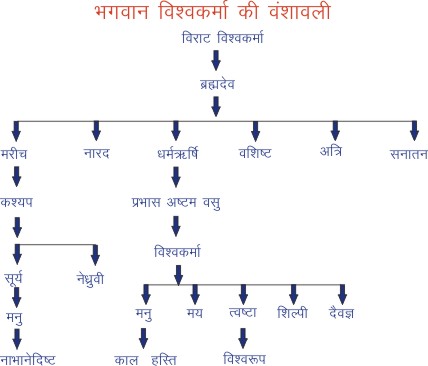
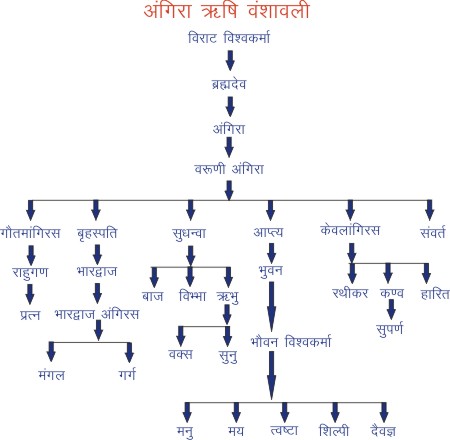
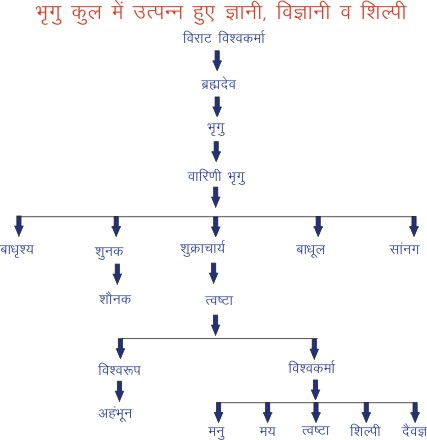
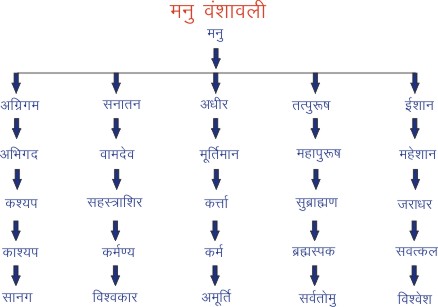
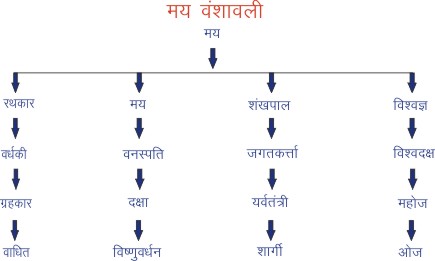
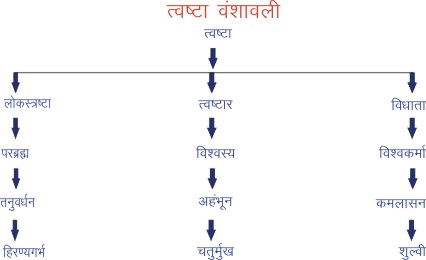
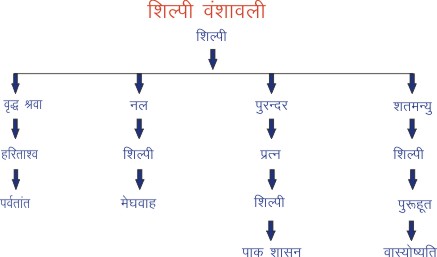
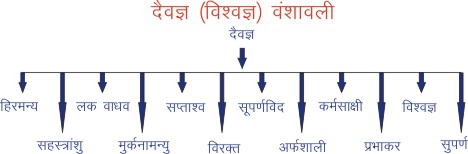 वेदों में विश्वकर्मा
वेदों में विश्वकर्मा